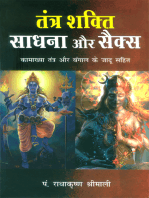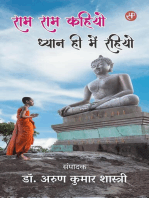Professional Documents
Culture Documents
तन्त्रयुक्ति - विकिपीडिया
तन्त्रयुक्ति - विकिपीडिया
Uploaded by
Nandakishor Mansure100%(1)100% found this document useful (1 vote)
354 views15 pagesPadaarth vigyan tantra yukti
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPadaarth vigyan tantra yukti
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
Download as pdf or txt
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
354 views15 pagesतन्त्रयुक्ति - विकिपीडिया
तन्त्रयुक्ति - विकिपीडिया
Uploaded by
Nandakishor MansurePadaarth vigyan tantra yukti
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
Download as pdf or txt
You are on page 1of 15
तन्त्रयुक्ति
तंत्रयुक्ति (६०० ईसा पूर्व) रचित एक भारतीय ग्रन्थ है
जिसमें परिषदों एवं सभाओं में शास्त्रार्थ (debate)
करने की विधि वर्णित है। वस्तुतः तंत्रयुक्ति हेतुविद्या
(logic) का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसका उल्लेख
चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अर्थशास्त्र ग्रन्थ,
विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि ग्रन्थों में भी मिलता है।[1]
किन्तु इसका सर्वाधिक उपयोग न्यायसूत्र एवं उसके
भाष्यों में हुआ है। सुश्रुतसंहिता के उत्तरतन्त्र में कहा
गया है कि युक्तितंत्र की सहायता से कोई अपनी बात
मनवा सकता है और विरोधी के तर्क को गलत सिद्ध कर
सकता है।
तन्त्रयुक्ति एक उपकरण है जो किसी ग्रन्थ की रचना
करते समय अत्यन्त उपयोगी होता है। निम्नलिखित
श्लोक तन्त्रयुक्ति के ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करता है-
अधीयानोऽपि तन्त्राणि तन्त्रयुक्त्यविचक्षणः।
नाधिगच्छति तन्त्रार्थमर्थं भाग्यक्षये यथा॥
(सर्वाङसुन्दरा पृष्ट ९२)
(अर्थ : जिस प्रकार भाग्य के क्षय होने पर व्यक्ति को
अर्थ (धन) की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार यदि
किसी ने तन्त्र (शास्त्र) का अध्ययन किया है किन्तु वह
तन्त्रयुक्ति का उपयोग करना नहीं जानता तो वह
शास्त्र का अर्थ नहीं समझ पाता है।)
चरकसंहिता में ३६ तंत्रयुक्तियाँ गिनाई गयीं हैं।[2]
तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽर्थः पदस्य च ४१
प्रदेशोद्देशनिर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम्
उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णयाः ४२
प्रसङ्गैकान्तनैकान्ताः सापवर्गो विपर्ययः
पूर्वपक्षविधानानुमतव्याख्यानसंशयाः ४३
अतीतानागतावेक्षास्वसंज्ञोह्यसमुच्चयाः
निदर्शनं निर्वर्चनं संनियोगो विकल्पनम् ४४
प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः
(१) अधिकरण (२) योग (३) हेत्वर्थ (४) पदार्थ (५)
प्रदेश (६) उद्देश (७) निर्देश (८) वाक्यशेष
(९) प्रयोजन (१०) उपदेश (११) अपदेश (१२)
अतिदेश (१३) अर्थापत्ति (१४) निर्णय (१५) प्रसङ्ग
(१६) एकान्त
(१७) अनैकान्त (१८) अपवर्ग (१९) विपर्यय (२०)
पूर्वपक्ष (२१) विधान (२२) अनुमत (२३) व्याख्यान
(२४) संशय
(२५) अतीतावेक्षण (२६) अनागतावेक्षण (२७)
स्वसंज्ञा (२८) ऊह्य (२९) समुच्चय (३०) निदर्शन
(३१) निर्वचन (३२) संनियोग
(३३) विकल्पन (३४) प्रत्युत्सार (३५) उद्धार (३६)
सम्भव ।
अष्टांगहृदय में भी इन ३६ तन्त्रयुक्तियों को गिनाया गया
है। सुश्रुतसंहिता के ६५वें अध्याय में ३२ तन्तयुक्तियाँ
गिनायी गयीं हैं। अर्थशास्त्र के १५वें अधिकरण में
चाणक्य ने ३२ तन्त्रयुक्तियाँ गिनायीं हैं।[3] वे कहते हैं कि
उनके इस ग्रन्थ को समझने के लिए ये ३२ तन्त्रयुक्तियाँ
बहुत उपयोगी हैं। कौटिल्य द्वारा गिनायी गयीं ३२
तन्त्रयुक्तियाँ अधिकांशतः सुश्रुत द्वारा गिनाए गये ३२
तन्त्रयुक्तियों से बहुत मिलतीं हैं।
तन्त्रयुक्ति के उपयोग
संक्षेप में, तन्त्रयुक्ति के मुख्यतः दो उपयोग हैं-
(अत्रासां तन्त्रयुक्तीनां किं प्रयोजनम्? उच्यते-
वाक्ययोजनमर्थयोजनं च ॥४॥)
(१) वाक्ययोजन -- वाक्यों का उचित संयोजन
(२) अर्थयोजन -- अर्थ का सही ढंग से प्रस्तुतीकरण
या विन्यास
असद्वादिप्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् ।
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥५॥
व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यार्था लीना ये चाप्यनिर्मलाः ।
लेशोक्ता ये च के चित्स्युस्तेषां चापि प्रसाधनम् ॥६॥
यथाऽम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा ।
प्रबोधस्य प्रकाशार्थं तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥७॥
(तन्त्रयुक्त्यध्यायः / सुश्रुतसंहिता )
तन्त्रयुक्ति उनका भी अर्थ स्पष्ट कर देती है जो-
अव्यक्त
अनुक्त
लीनार्थ
अनिर्मलार्थ
लेषोक्त
होते हैं।[4]
तन्त्रयुक्ति तथा वैज्ञानिक और सैद्धांतिक ग्रंथों
की रचना
एक व्यवस्थित ग्रन्थ की संरचना के लिए सभी मूलभूत
पहलू तन्त्रयुक्ति में शामिल हैं। इसको ग्रन्थ की
आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है।
सभी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक ग्रंथों की रचना पद्धति के
रूप में तन्त्रयुक्ति 1500 से अधिक वर्षों के लिए
प्रभावशाली थी। इसका अखिल भारतीय प्रसार था।
ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात १२वीं
शताब्दी तक (लगभग 1500 वर्ष) संस्कृ त वाङ्मय में हम
तन्त्रयुक्तियों के संदर्भ पाते हैं। ऐसा ग्रंथ रचना पद्धति जो
इतने लंबे समय से प्रचलन में थी , गैर-उपयोग में आ
गया और फलस्वरूप उसे भुला दिया गया।
निम्नलिखित सारणी तन्त्रयुक्ति के उपयोगों को सार रूप
में प्रस्तुत करती है-[5]
क्रम
उपयोगिता-क्षेत्र तन्त्रयुक्ति
संख्या
१ ग्रन्थ की मूलभूत संरचना प्रयोजन, अधिकरण, विधान, योग, उद्देश, निर्देश
नियोग, अपवर्ग, विकल्पन, उपदेश, स्वसंज्ञा, निर्णय, प्रसङ्ग, एकान्त,
२ सिद्धान्त एवं नियमों का कथन
अनेकान्त, विपर्यय
विभिन्न संकल्पनाओम की व्याख्या निर्वचन, पूर्वपक्ष, अनुमत, व्याख्यान, निदर्शन, हेत्वार्थ, अपदेश, अतिदेश,
३
और विस्तार उह्य
ठीक-ठीक सम्पादन तथा अभिव्यक्ति वाक्यशेष, अर्थापत्ति, समुच्चय, पदार्थ, अतीतवेक्षण, अनागतवेक्षन, प्रदेश,
४
की शैली प्रत्युत्सर, उद्धार, सम्भव
तन्त्रयुक्तियों का संक्षिप्त परिचय
अधिकरण ( Main Topic ) :- जिस मुुुख्य विषय को
लेकर बाकी सब बाते कही जा रही है।
योग ( Correlation ) :- पहले वाक्य में कहे हुए शब्द
से दूसरे वाक्य में कहे गए शब्द से परस्पर संबंध होना,
अलग अलग कहे शब्दों का आपस में एकत्र होना योग
है।
पदार्थ :- किसी सूत्र में या किसी पद में कहा गया विषय
पदार्थ है।
हेत्वर्थ :- जो अन्यत्र कहा हुआ अन्य विषय का साधक
होता है, वह हेत्वर्थ है।
उद्देश्य :- संक्षेप में कहा गया विषय।
निर्देश :- विस्तार से कहा जाना निर्देश है।
अपदेश :- कार्य के प्रति कारण का कहा जाना अपदेश
कहा जाता है। जैसे :- मधुर रस सेवन से कफ की वृद्धि
होती है क्योंकि दोनों के गुण समान है।
प्रदेश:- अतीत अर्थ से साधन प्रदेश कहा जाता है।
अतिदेश :- प्रकृ त विषय से उसके सदृश अनागत विषय
का साधन अतिदेश कहा जाता है। जैसे :- आसमान
नीला होता है अगर इसके अलावा कोई और होगा तो
उसका साधन अतिदेश कहा जाएगा।
उपवर्ग :- सामान्य वचन के कथन से किसी का ग्रहण
और पुनः विशेष वचन से उसका कु छ निराकरण अपवर्ग
है।
वाक्य दोष :- जिस पद के कहे बिना ही वाक्य समाप्त
हो जाता है, वह वाक्यदोष कहा जाता है, पर यह वाक्य
दोष कार्य विषय का बोधक होता है । जैसे :- शरीर के
अंगो के नाम के साथ पुरुष का प्रयोग शरीर को दर्शाता
है वहीं के वल पुरुष का प्रयोग आत्मा का बोधक होता है।
अर्थापत्ति :- एक विषय के प्रतिपादन से अन्य
अप्रतिपादित विषय का स्वतः सिद्ध हो जाना अर्थात्
ज्ञान हो जाना अर्थापति कहलाता है।
विपर्यय :- जो कहा जाये, उससे विपरीत ‘विपर्यय’ कहा
जाता है।
प्रसङ्ग :- दूसरे प्रकरण से विषय की समाप्ति अथवा
प्रथम कथित विषय के प्रकरण में आ जाने से उसे पुनः
कहना प्रसंग कहा जाता है।
एकान्त :- जो सर्वत्र एक समान कहीं गई बात है। जैसे
मदन फल का वमन में उपयोग।
अनेकान्त :- कहीं किसी का कु छ कहना कहीं कु छ।
जहां पर आचार्यों के बीच में मतभेद हो। जैसे :- रस
संख्या की संभाषा में अलग-अलग आचार्यों के रस की
संख्या अलग-अलग थी।
पूर्वपक्ष :- आक्षेप पूर्वक प्रश्न करना। जैसे :- क्यों वात
जनित प्रमेह असाध्य होते हैं।
निर्णय :- पूर्वपक्ष का जो उत्तर होता है वही निर्णय है।
अनुमत-लक्षण :- दूसरे के मत का भिन्न होने पर
प्रतिषेध न करना ‘अनुमत’ कहलाता है। जैसे कोई कहे
रस की संख्या 7 है ( आचार्य हारित ने भी रस 7 माने है
)।
विधान :- प्रकरण के अनुपूर्वक्रम ( यथाक्रम ) से कहा
गया विधान है।
अनागतावेक्षण :- भविष्य में अर्थात् आगे कहा जाने
वाला विषय।
अतिक्रान्तावेक्षण :- जो विषय प्रथम कहा गया हो, उस
पर पुनः विचार करना अतिक्रान्तावेक्षण कहा जाता है।
संशय :- दोनों प्रकार के हेतुओं का दिखलायी देना
संशय कहा जाता है। जैसे :- कोई ऐसा विषय जिसमें
समझ में नहीं आए की यह करना है अपितु नहीं करना।
व्याख्यान :- शास्त्र में विषय का अतिशय रूप से
सम्यकृ तया समझाकर वर्णन करना व्याख्यान कहा
जाता है। जैसे :- आयुर्वेद संहिता में रोगों की चिकित्सा
की व्याख्या की गई है।
स्वसंज्ञा :- किसी की अन्य शास्त्रों से भिन्न जो अपनी
संज्ञा दी जाती है। जैसे :- मिश्रक वर्गीकरण अलग अलग
आचार्यों ने एक साथ योगों को अपने अपने नाम दिए है।
निर्वचन :- निश्चित वचन कहना निर्वाचन कहा जाता है।
जैसे रस की संख्या 6 है।
निदर्शन :- जिस वाक्य में दृष्टान्त से विषय व्यक्त किया
गया हो, वह निदर्शन है।
नियोग :- यह ही करना है यह नियोग है। जैसे पथ्य का
ही सेवन करना है।
समुच्चय :- यह और यह इस प्रकार कहना समुच्चय है।
जैसे :- सब बा तों को इकठ्ठा करके कहना।
विकल्प :- यह अथवा यह–इस प्रकार का वाक्य अथवा
कहकर कहा जाना ‘विकल्प’ कहलाता है।
ऊह्म :- शास्त्र में अनिर्दिष्ट विषय को बुद्धि से तर्क कर
जो जाना जाता है। जैसे :- किसी रोग में उपद्रव होने
का कारण जानना।
प्रयोजन :- जिस विषय की कामना करते हुए उसकी
सम्पन्नता में कर्ता प्रवृत्त होता है, वह प्रयोजन है।
प्रत्युत्सार :- प्रमाण एवं युक्ति द्वारा दूसरे के मत का
निवारण करना ‘प्रत्युत्सार’ कहा जाता है। जैसे भगवान
पुनर्वसु ने रस की संख्या निर्धारण से पहले सभी
आचार्यों के प्रति उत्तर दिए थे।
उद्धार :- दूसरे के पक्ष में दोष निकाल कर अपना पक्ष
सिद्ध करना।
सम्भव :- जो जिसमें उपपद्यमान होता है, वह उसका
‘सम्भव’ है।
इन्हें भी देखें
वादविद्या
न्यायसूत्र
आन्वीक्षिकी (अर्थात् 'अन्वेषण विज्ञान')
वाद-विवाद
शास्त्रार्थ
न्याय (दृष्टांत वाक्य)
वैज्ञानिक विधि
You might also like
- Hindu Darshan in Hindi by S. RadhakrishnanDocument68 pagesHindu Darshan in Hindi by S. RadhakrishnankartikscribdNo ratings yet
- Tantra Shakti, Sadhna aur Sex (तंत्र शक्ति साधना और सैक्स)From EverandTantra Shakti, Sadhna aur Sex (तंत्र शक्ति साधना और सैक्स)Rating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (26)
- Sri Hari AshtakamDocument5 pagesSri Hari AshtakamKs Krishnans0% (1)
- Tark SangrahDocument98 pagesTark SangrahSher SinghNo ratings yet
- पुरुषार्थ, अध्याय 3Document38 pagesपुरुषार्थ, अध्याय 3Saif AliNo ratings yet
- हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।Document15 pagesहिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।sable1804No ratings yet
- Patanjali Yoga Sutra HindiDocument159 pagesPatanjali Yoga Sutra HindiAnonymous eKt1FCDNo ratings yet
- दर्शनDocument5 pagesदर्शनLokesh GautamNo ratings yet
- Kshtaksheena Chikitsa Adyaya No 11Document35 pagesKshtaksheena Chikitsa Adyaya No 11Shantu ShirurmathNo ratings yet
- Panchkarma Slokavali by Dr. AmiyaDocument2 pagesPanchkarma Slokavali by Dr. Amiyavarunn100% (2)
- The Concept of Ashta Vidha Shastra Karma Is A Unique Contribution of Acharya Sushruta. These EightDocument43 pagesThe Concept of Ashta Vidha Shastra Karma Is A Unique Contribution of Acharya Sushruta. These Eightbharti guptaNo ratings yet
- JwaraDocument9 pagesJwaraRandeep ChaudharyNo ratings yet
- 4 - VigyanMaya - KoshDocument16 pages4 - VigyanMaya - Koshcfcs100% (1)
- Kanak DharaDocument19 pagesKanak Dharavimal vyasNo ratings yet
- Navya Nyaya Bhasha PradipaDocument2 pagesNavya Nyaya Bhasha PradipaChandrashekar Ramaswamy50% (2)
- श्री विन्ध्येश्वरी स्तोत्रमDocument4 pagesश्री विन्ध्येश्वरी स्तोत्रमSukantaNo ratings yet
- JwaraDocument33 pagesJwara19 Yash LadNo ratings yet
- संस्कृत सुभाषितानि subashitanam snagrhaDocument17 pagesसंस्कृत सुभाषितानि subashitanam snagrhaAnonymous 3pTM9WCY0% (1)
- Koshtha AyurvedaDocument7 pagesKoshtha AyurvedaAnamika SrivastavaNo ratings yet
- उपनिषद्Document11 pagesउपनिषद्Rohit SahuNo ratings yet
- अनुमान प्रमाणDocument56 pagesअनुमान प्रमाणsable1804No ratings yet
- सनातन धर्म-2 hindi 2ndDocument32 pagesसनातन धर्म-2 hindi 2ndSarthak MeenaNo ratings yet
- Kushtha RogDocument26 pagesKushtha Rogaman tyagi0% (1)
- Sangya PrakaranDocument26 pagesSangya Prakarankishancreative18No ratings yet
- 02. भाषाओं का वर्गीकरणDocument21 pages02. भाषाओं का वर्गीकरणvishal sharmaNo ratings yet
- निर्वाण षट्कम PDFDocument1 pageनिर्वाण षट्कम PDFPrivate Tutor FlatNo ratings yet
- 2 - Pranmaya KoshDocument12 pages2 - Pranmaya KoshcfcsNo ratings yet
- धातुरूपDocument31 pagesधातुरूपsreevidhya KVNo ratings yet
- Shiv Panchakshar Stotra Meaning PDFDocument2 pagesShiv Panchakshar Stotra Meaning PDFchaturvedisureshraju7676100% (1)
- AsthiDocument25 pagesAsthiSiddhartha YadavNo ratings yet
- प्रत्ययDocument12 pagesप्रत्ययSandip KumarNo ratings yet
- Chandi KavachDocument5 pagesChandi KavachArun NaikNo ratings yet
- चार्वाक दर्शन PDFDocument10 pagesचार्वाक दर्शन PDFAvinashNo ratings yet
- Manomay KoshDocument10 pagesManomay KoshcfcsNo ratings yet
- रुद्रयामल उत्तर तंत्र योग साधनाDocument9 pagesरुद्रयामल उत्तर तंत्र योग साधनाyogender YogiNo ratings yet
- शिक्षाDocument26 pagesशिक्षाRohit SahuNo ratings yet
- Hindu DharmDocument3 pagesHindu DharmRafique MuhammadNo ratings yet
- शोध प्रयोगDocument40 pagesशोध प्रयोगsaraswatibooksagencyNo ratings yet
- निरुक्त नामक वेदांगःDocument25 pagesनिरुक्त नामक वेदांगःRohit SahuNo ratings yet
- Gherand Samhita - 1 IntroDocument13 pagesGherand Samhita - 1 IntroAnamika RawatNo ratings yet
- Document f829fc42Document15 pagesDocument f829fc42Pradeep ChoudharyNo ratings yet
- Mantra Anushthan Paddhati by Krishnanand Shastri (Missing Pages) Jalandhar - Bharatiya Sanskrit Bhavan - TextDocument440 pagesMantra Anushthan Paddhati by Krishnanand Shastri (Missing Pages) Jalandhar - Bharatiya Sanskrit Bhavan - Textविष्णु दत्त मिश्रNo ratings yet
- यज्ञ मीमांसाDocument15 pagesयज्ञ मीमांसाचन्द्रभाल सिंह86% (7)
- ईशावास्योपनिषद्Document42 pagesईशावास्योपनिषद्Arun Upadhyay100% (1)
- साधना में न्यास और उनके भेदDocument11 pagesसाधना में न्यास और उनके भेदgk_cosmicpower9No ratings yet
- Sankhya DarshanDocument28 pagesSankhya Darshanमयंक पाराशर100% (1)
- तत्त्वार्थ सूत्रDocument39 pagesतत्त्वार्थ सूत्रNaveen jainNo ratings yet
- योग के 20 सूत्रDocument9 pagesयोग के 20 सूत्रPriyedarshan GautamNo ratings yet
- पतंजलि सिलेबसDocument9 pagesपतंजलि सिलेबसvijay kumarNo ratings yet
- ।। तत्वार्थ सूत्र प्रश्नोत्तरी ।।Document148 pages।। तत्वार्थ सूत्र प्रश्नोत्तरी ।।Ujjwal JainNo ratings yet
- सांख्य साहित्य PDFDocument4 pagesसांख्य साहित्य PDFSurya Narayan Kumar Bhaskar100% (1)
- Unit - 1 To 8Document161 pagesUnit - 1 To 8Lâlû YâdâvNo ratings yet
- Tantra Sadhana Sar - Dev Dutt Shastri - TextDocument192 pagesTantra Sadhana Sar - Dev Dutt Shastri - TextSwapnil KulkarniNo ratings yet
- Ashtavakra GitaDocument105 pagesAshtavakra GitaRoy AnirbanNo ratings yet
- Hindi Presentation1Document3 pagesHindi Presentation1MakoNo ratings yet
- 1 Udgh ATanakavachastotramDocument5 pages1 Udgh ATanakavachastotramindira creationsNo ratings yet
- Prof - Rajesh Kumar Mishra Department of Philosophy Faculty of Humanites Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi-221002Document12 pagesProf - Rajesh Kumar Mishra Department of Philosophy Faculty of Humanites Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi-221002sachchidanand om Pathik (PAthik om)No ratings yet
- ManusmritiDocument122 pagesManusmritiPandit Janardan Mani Tiwari100% (1)